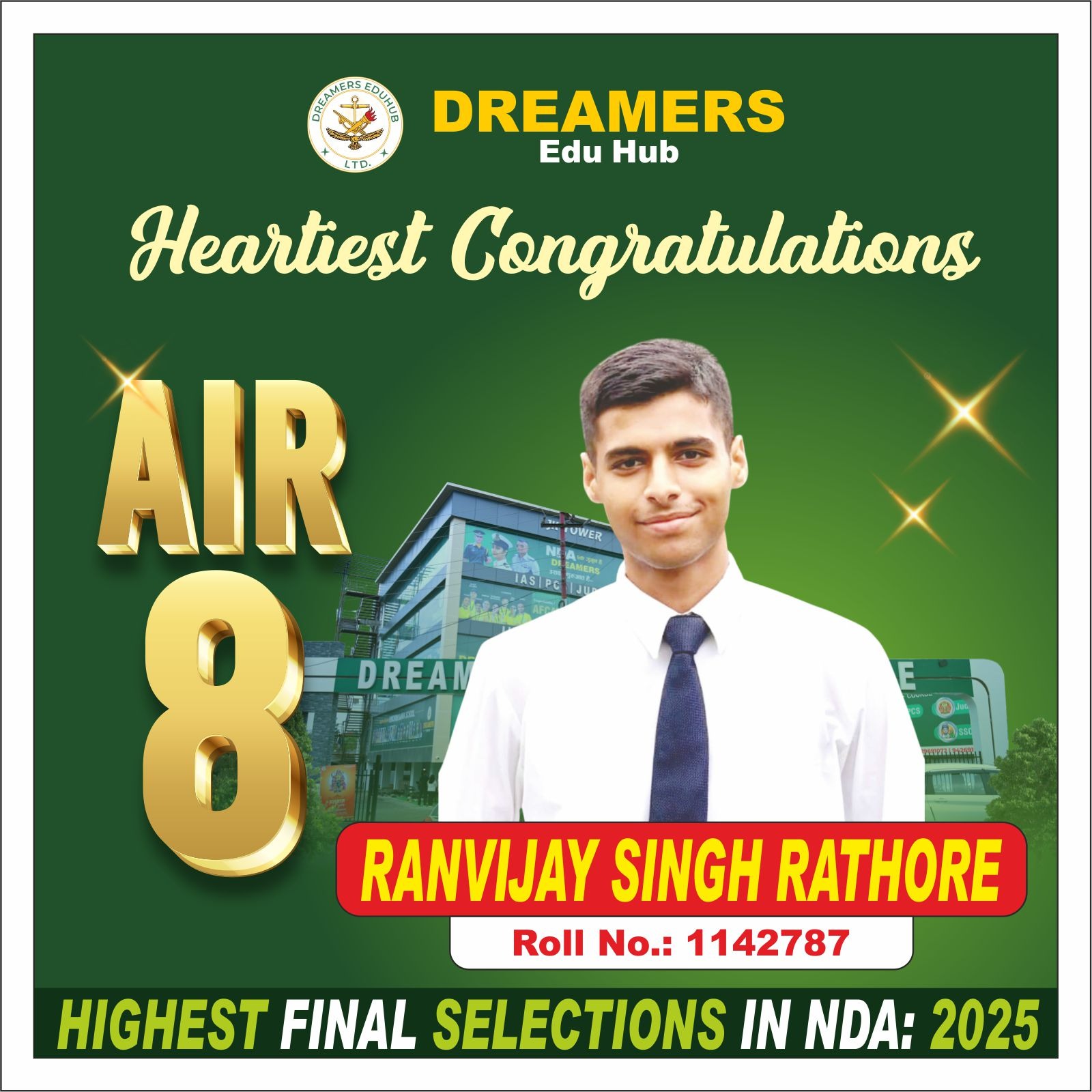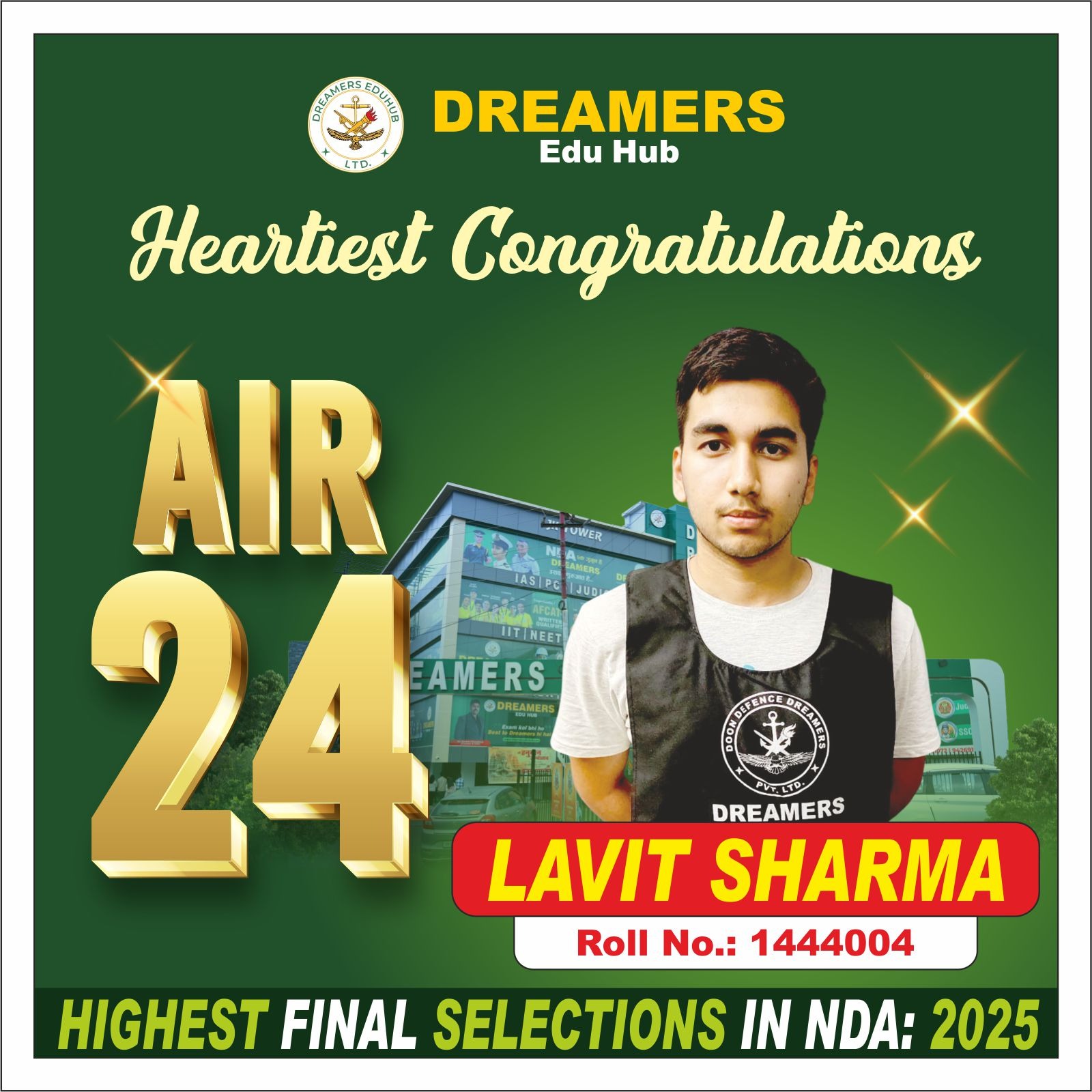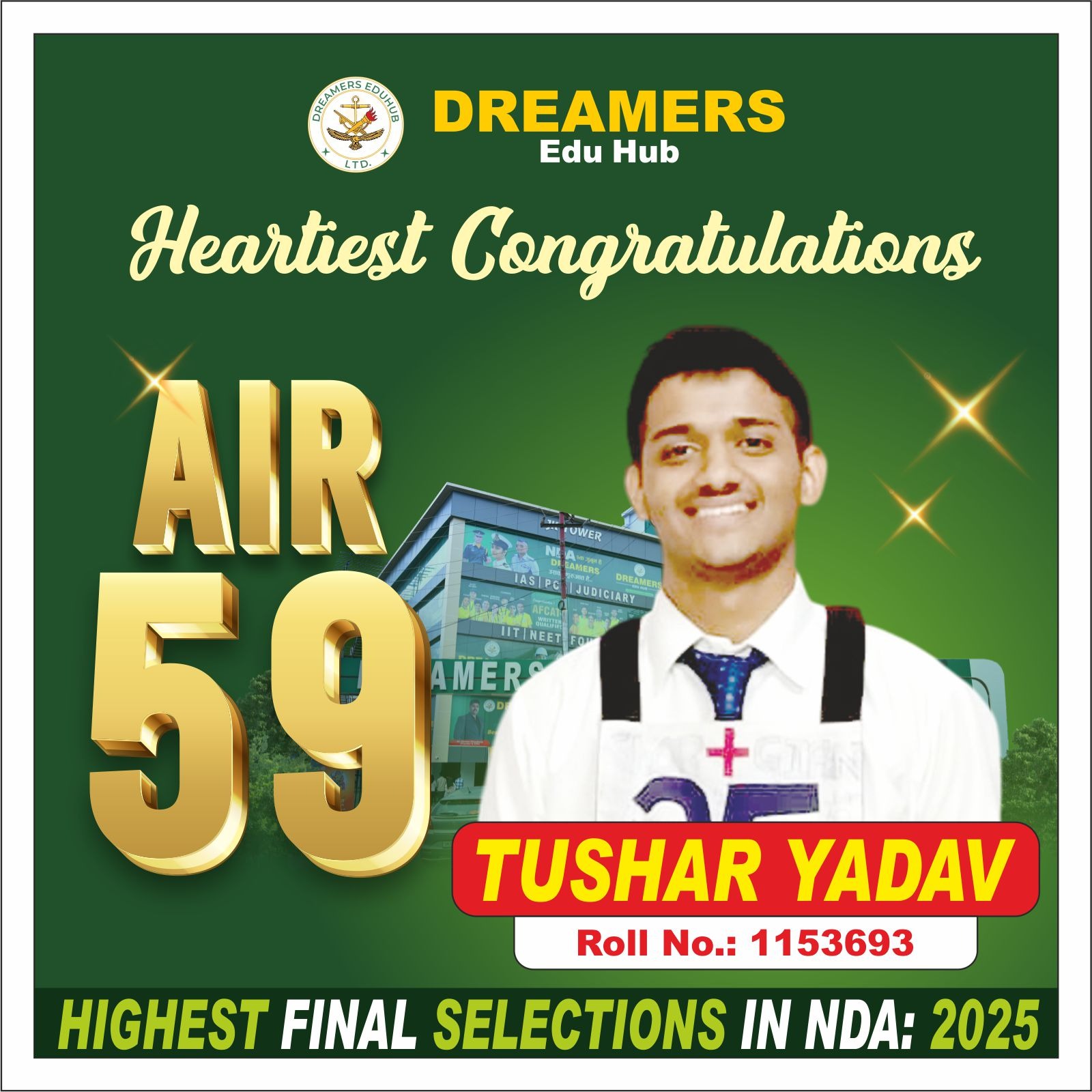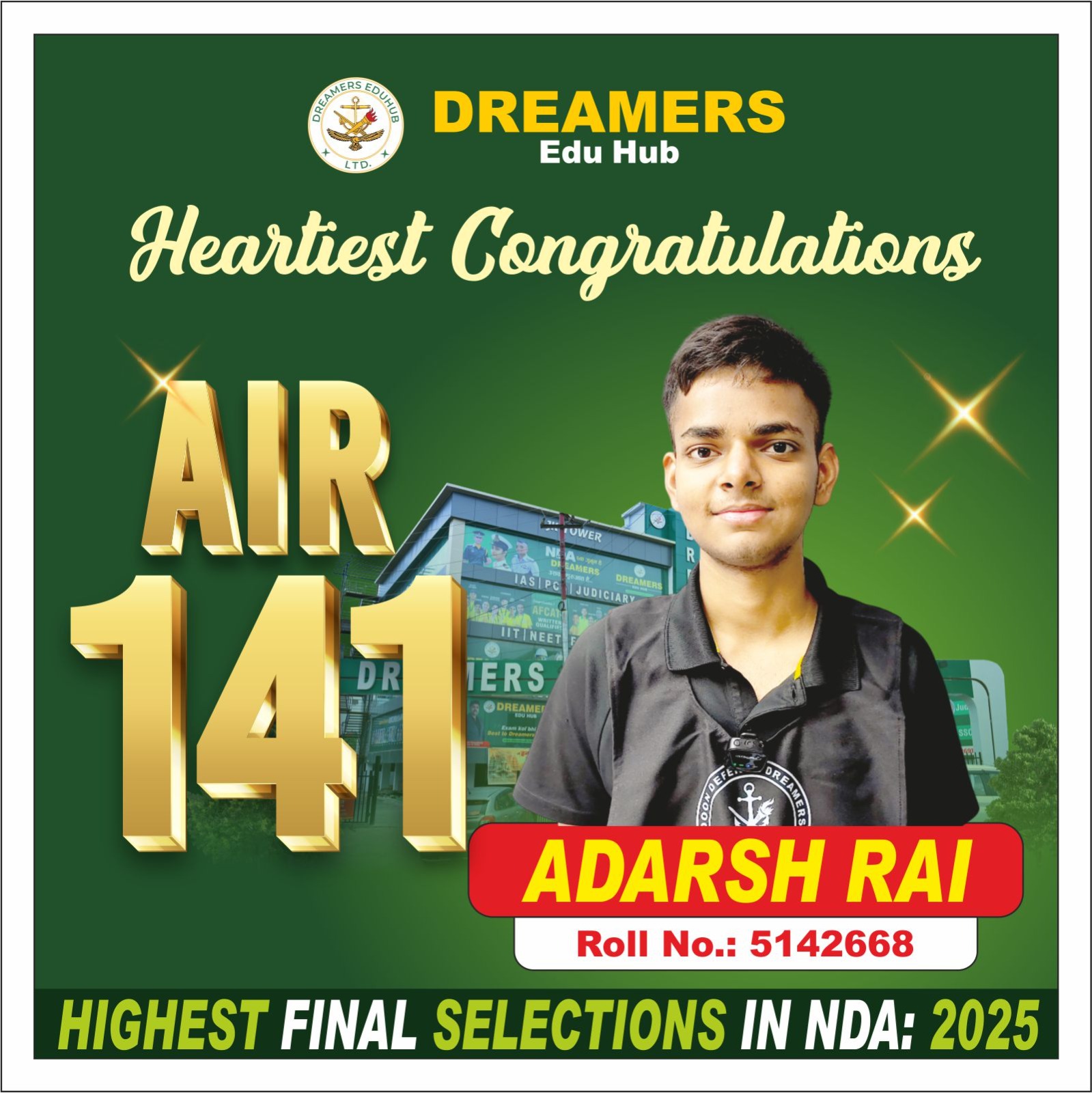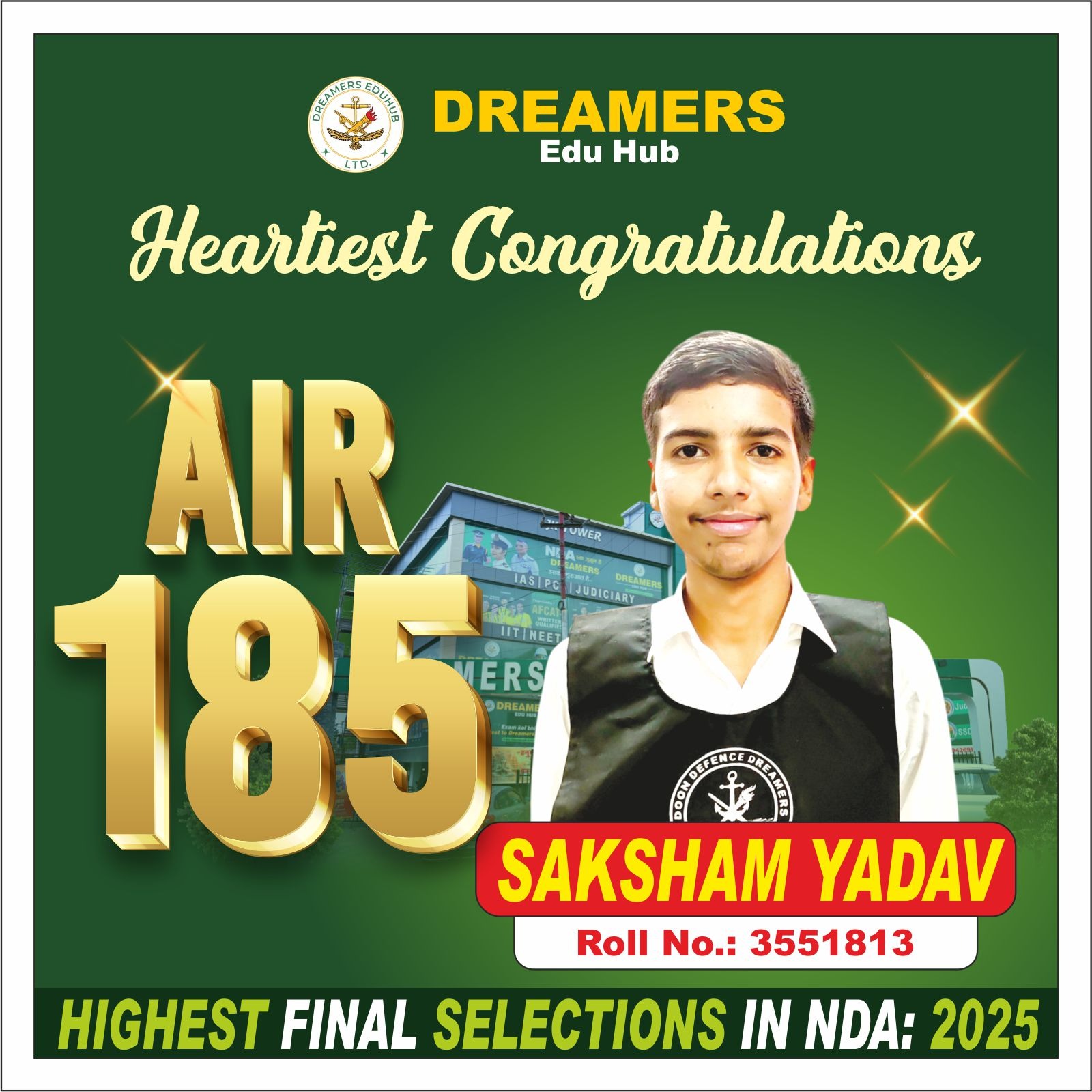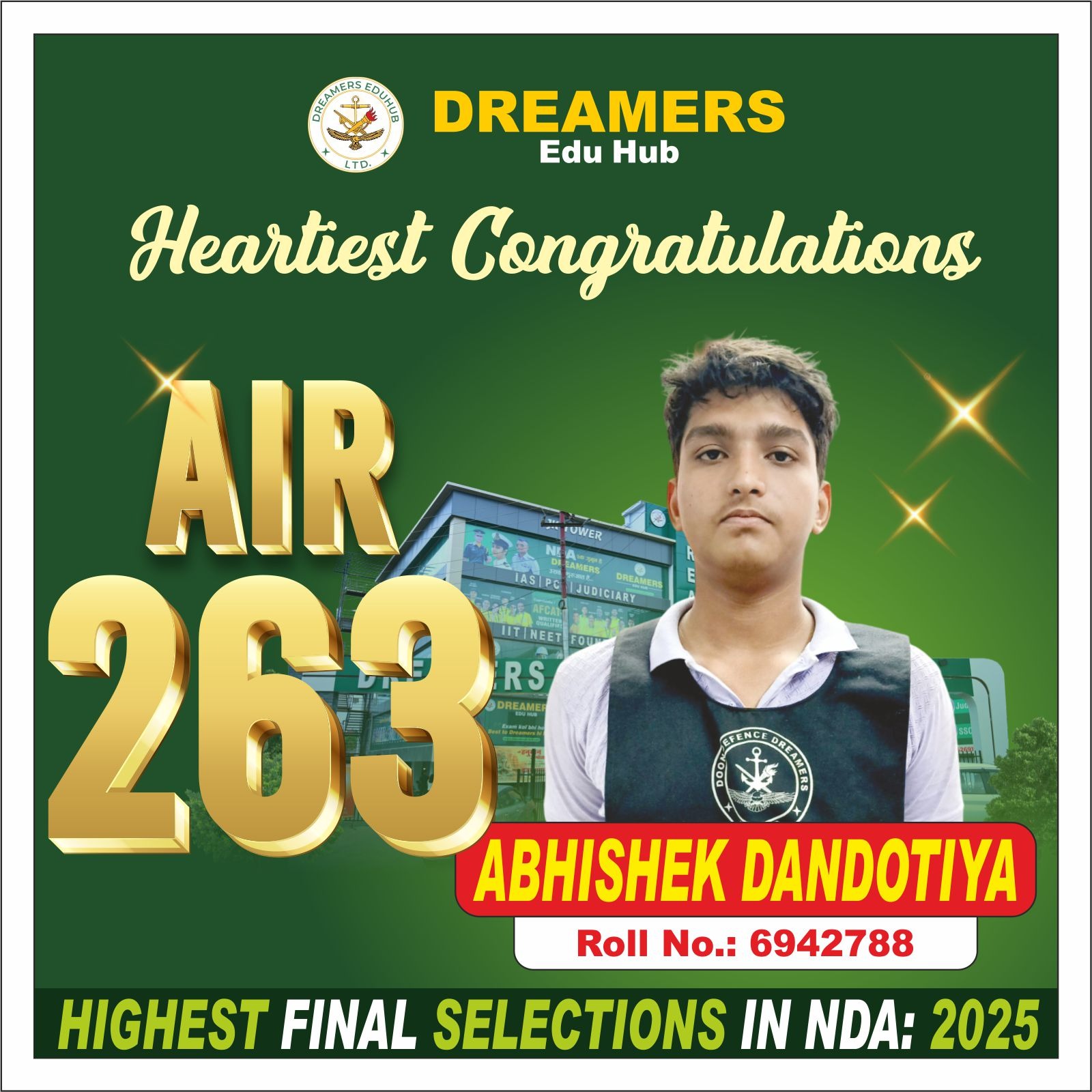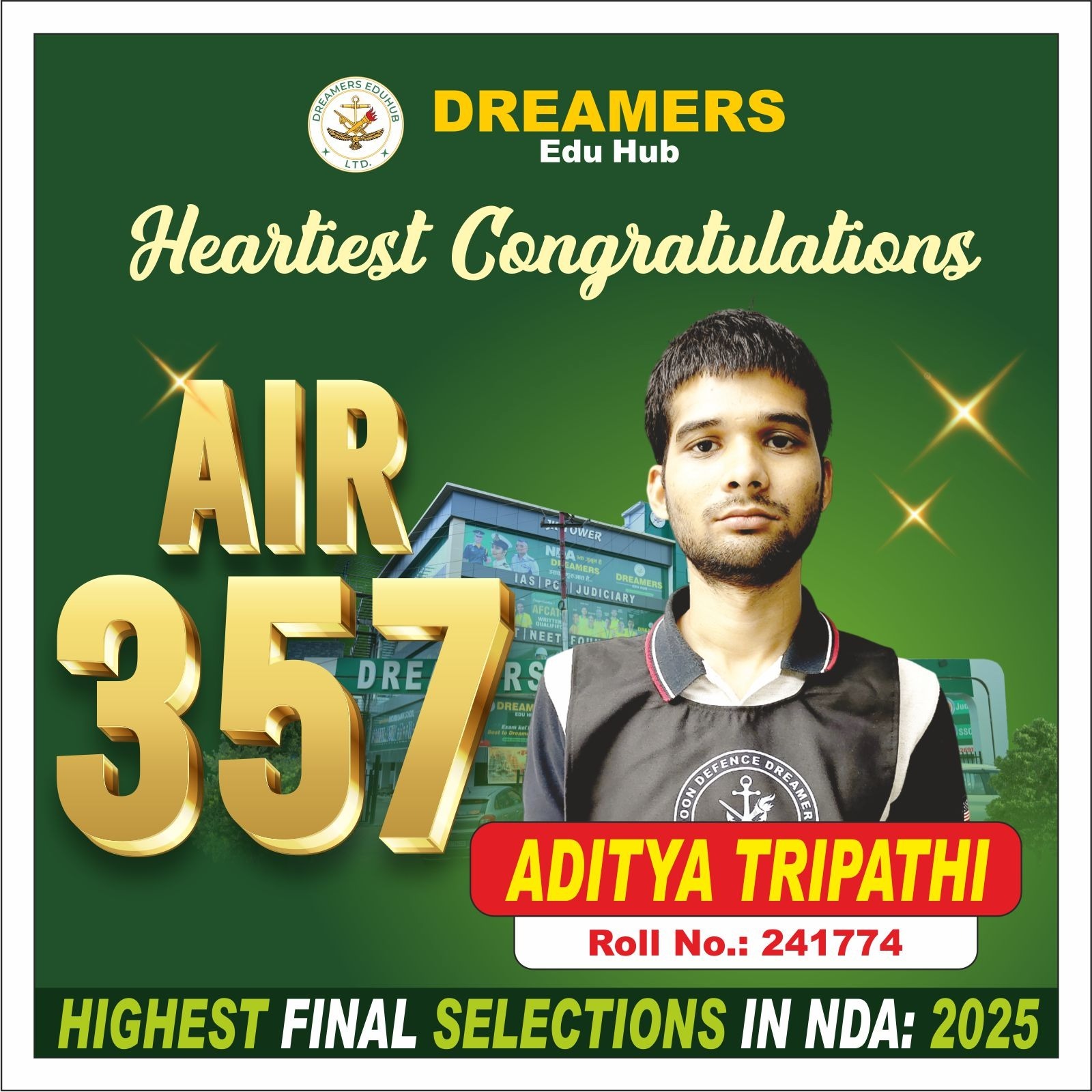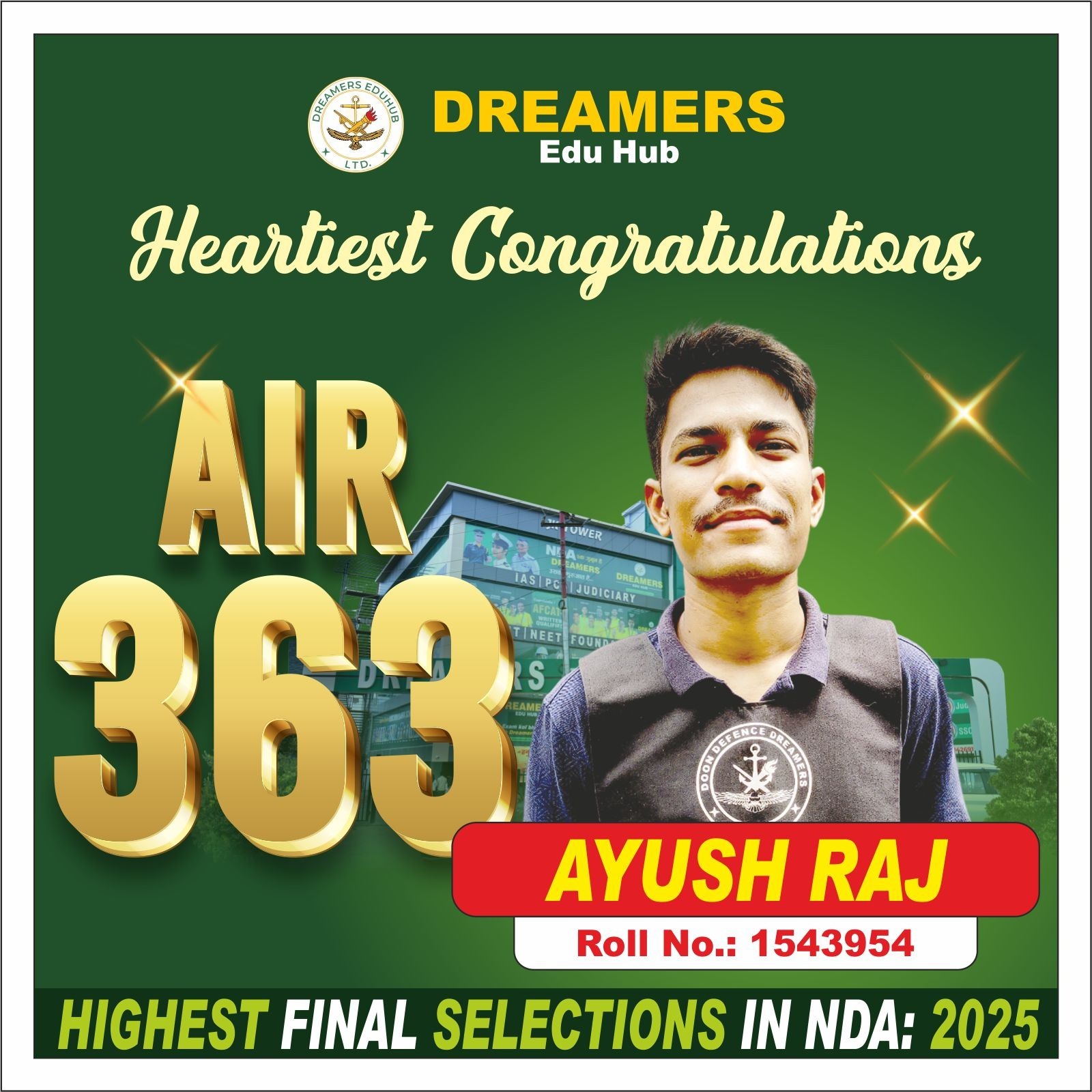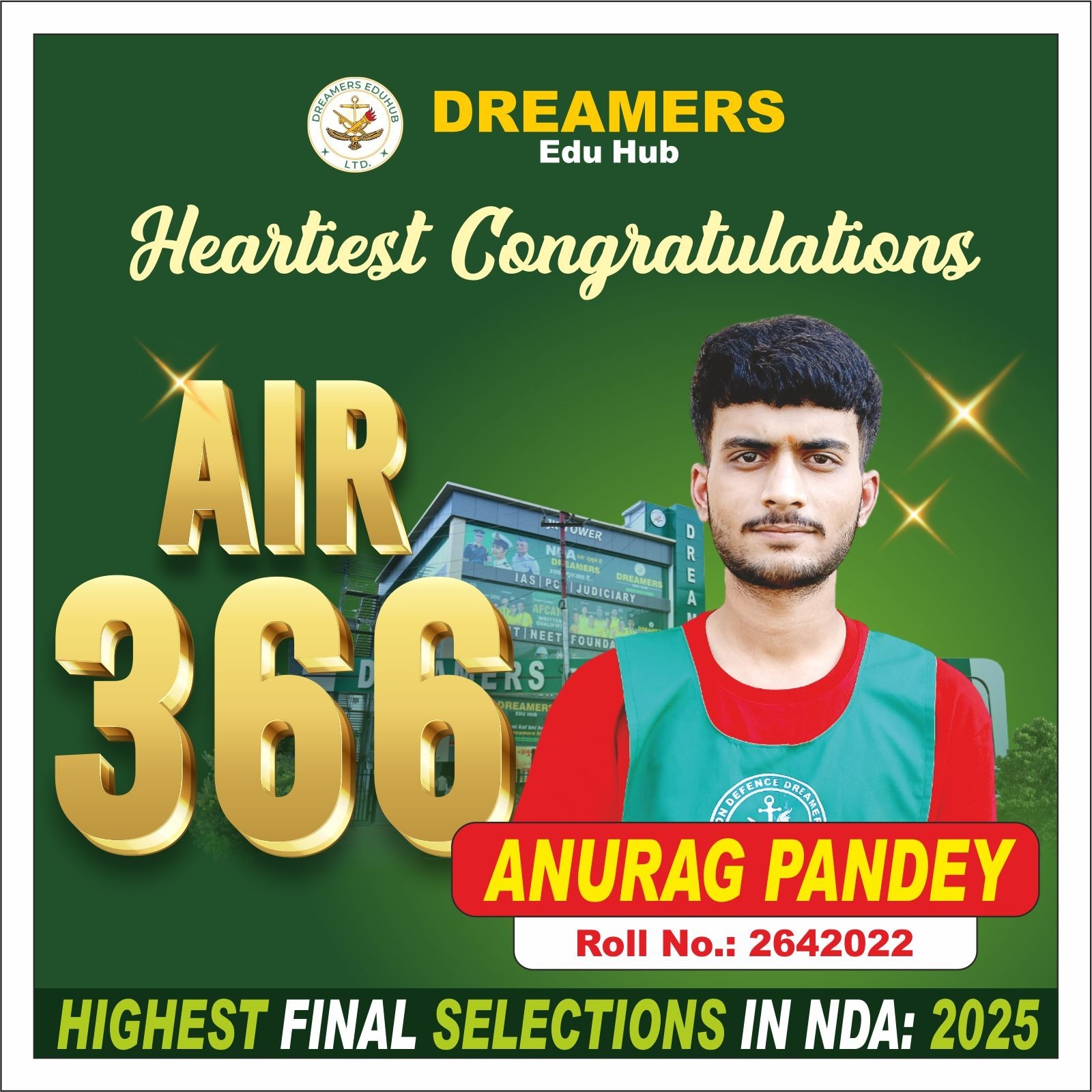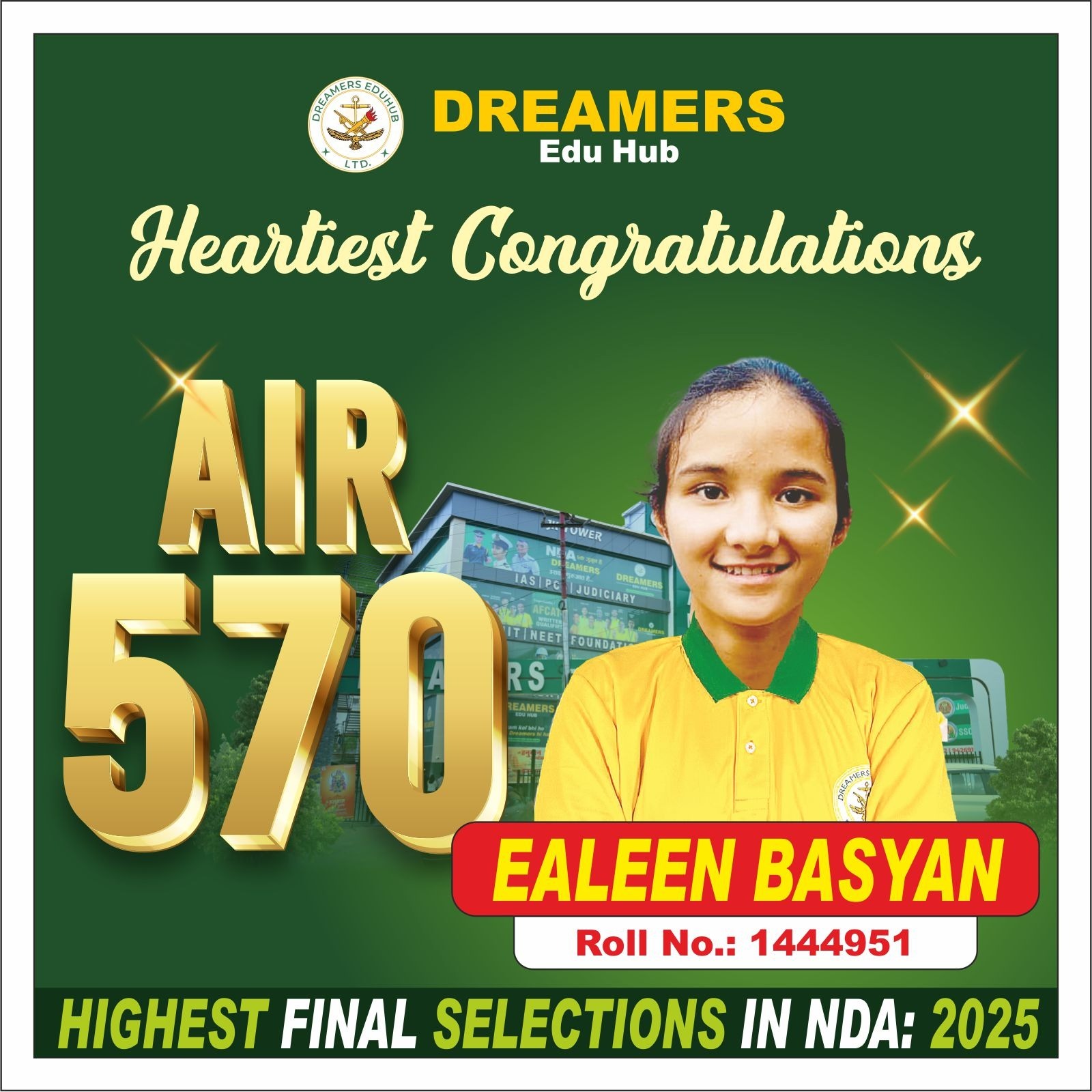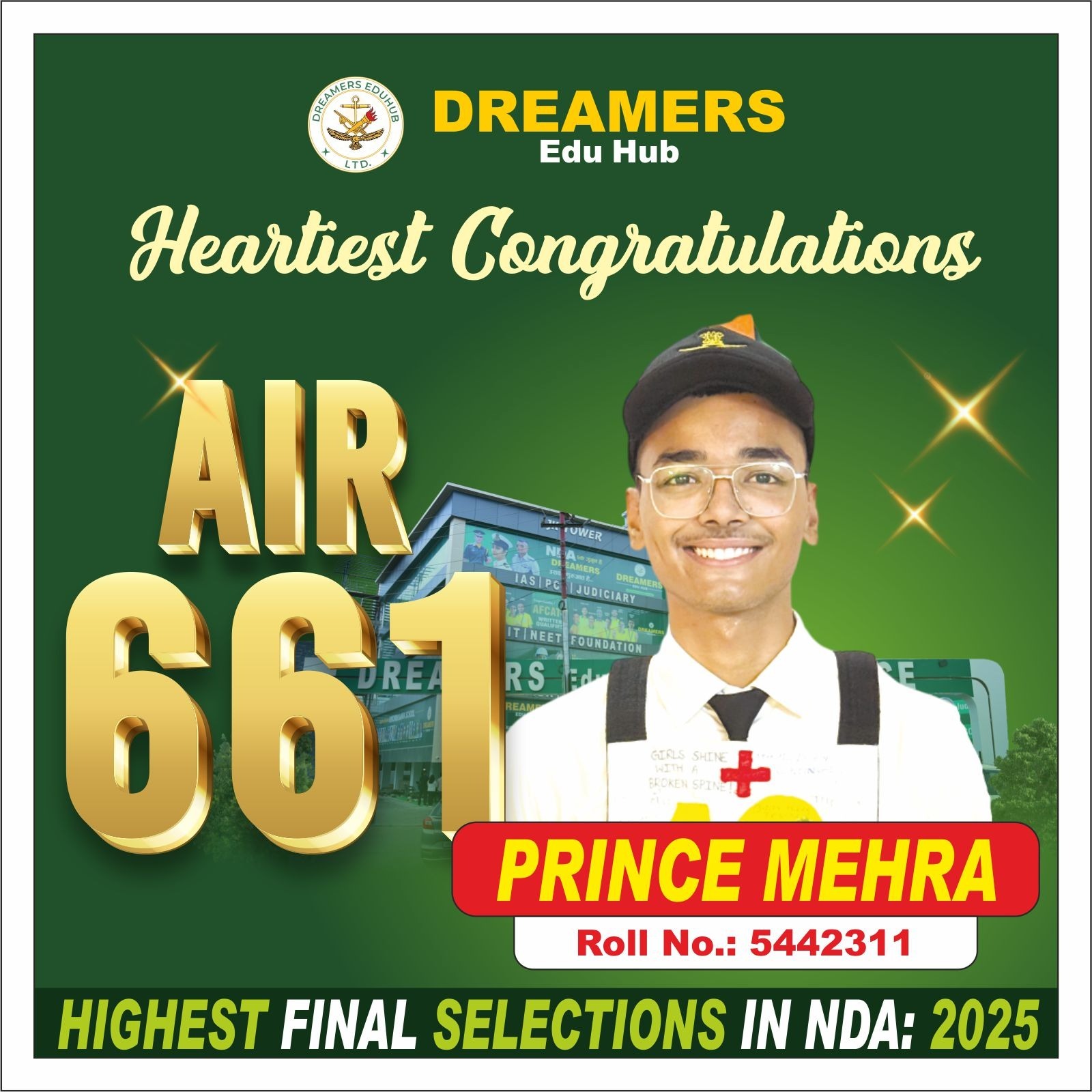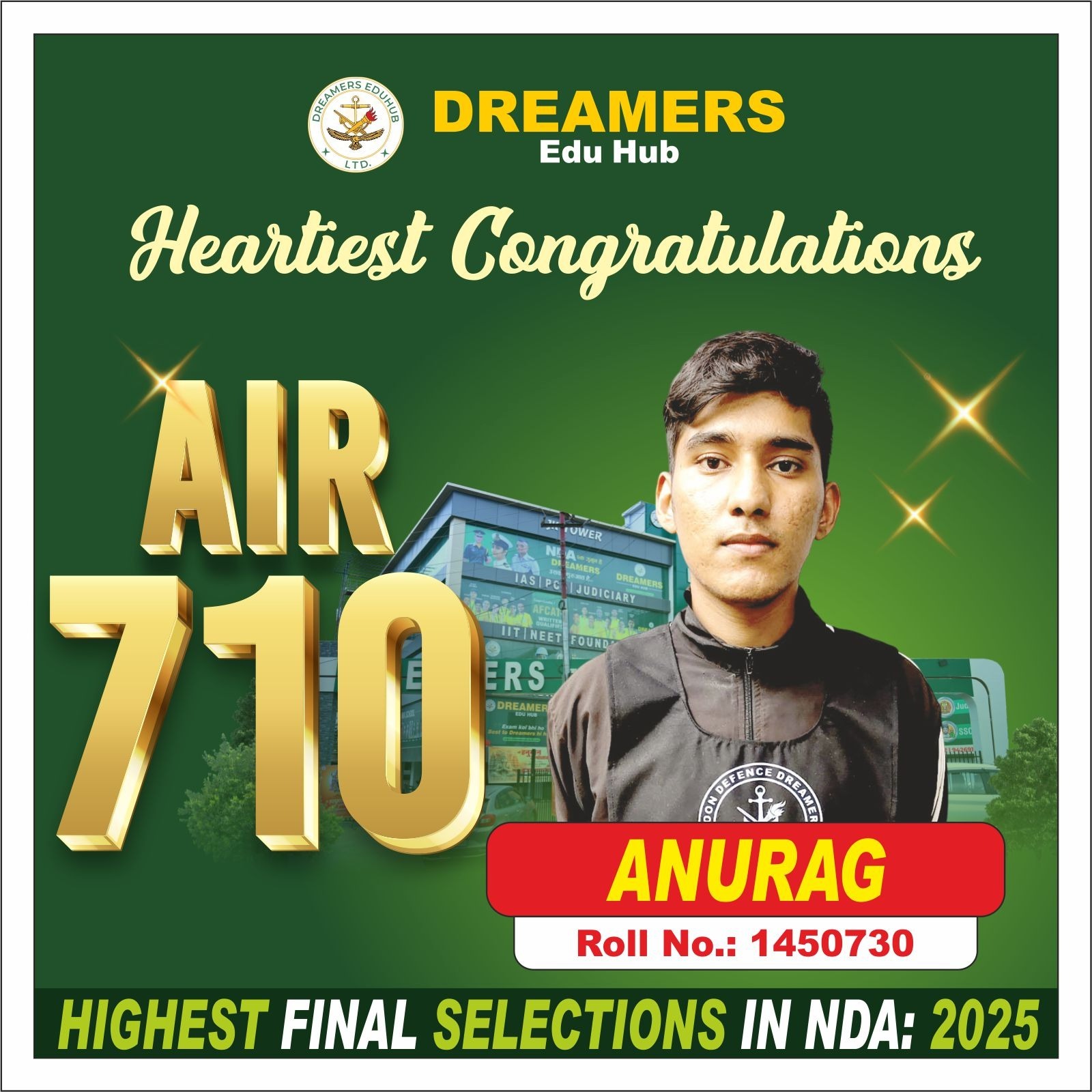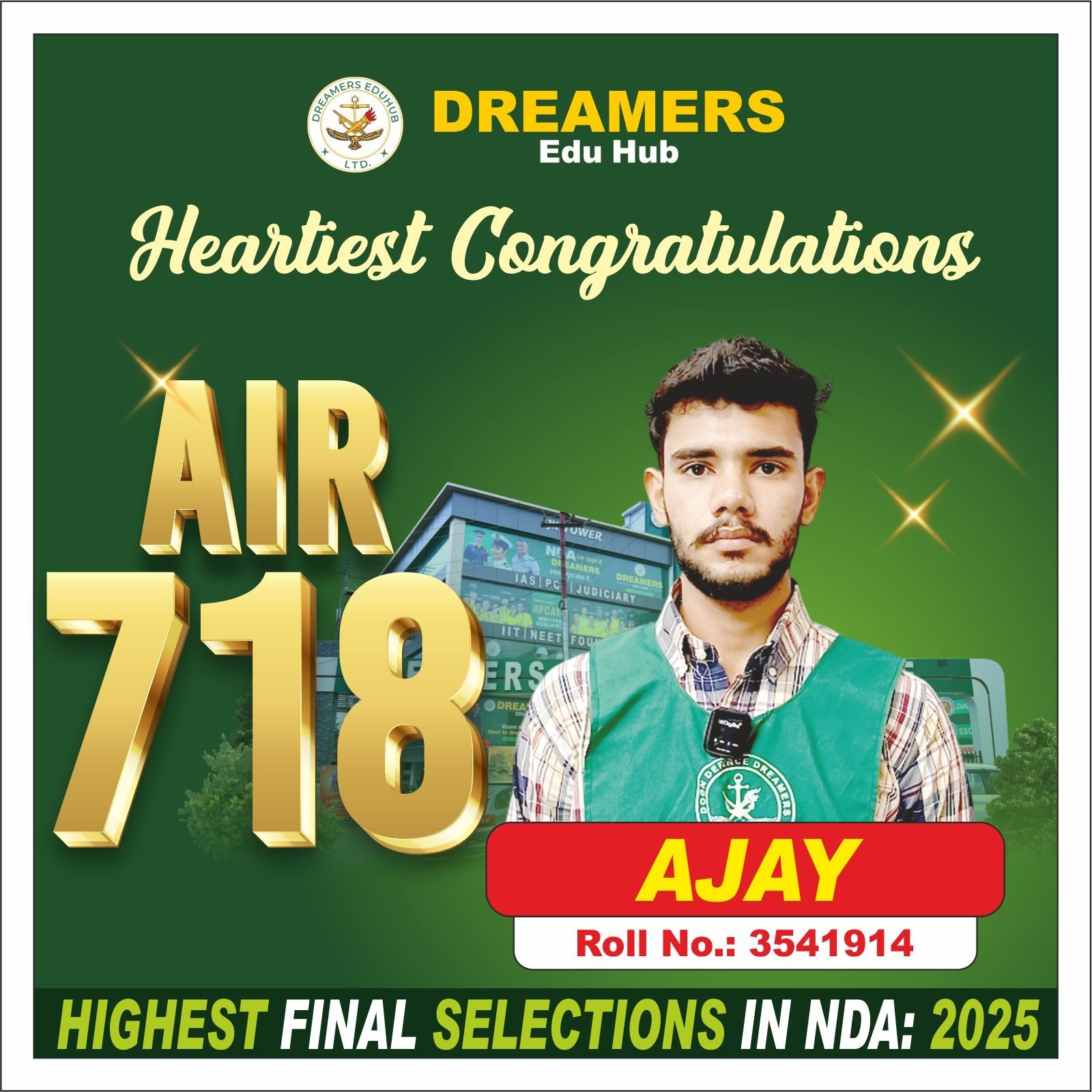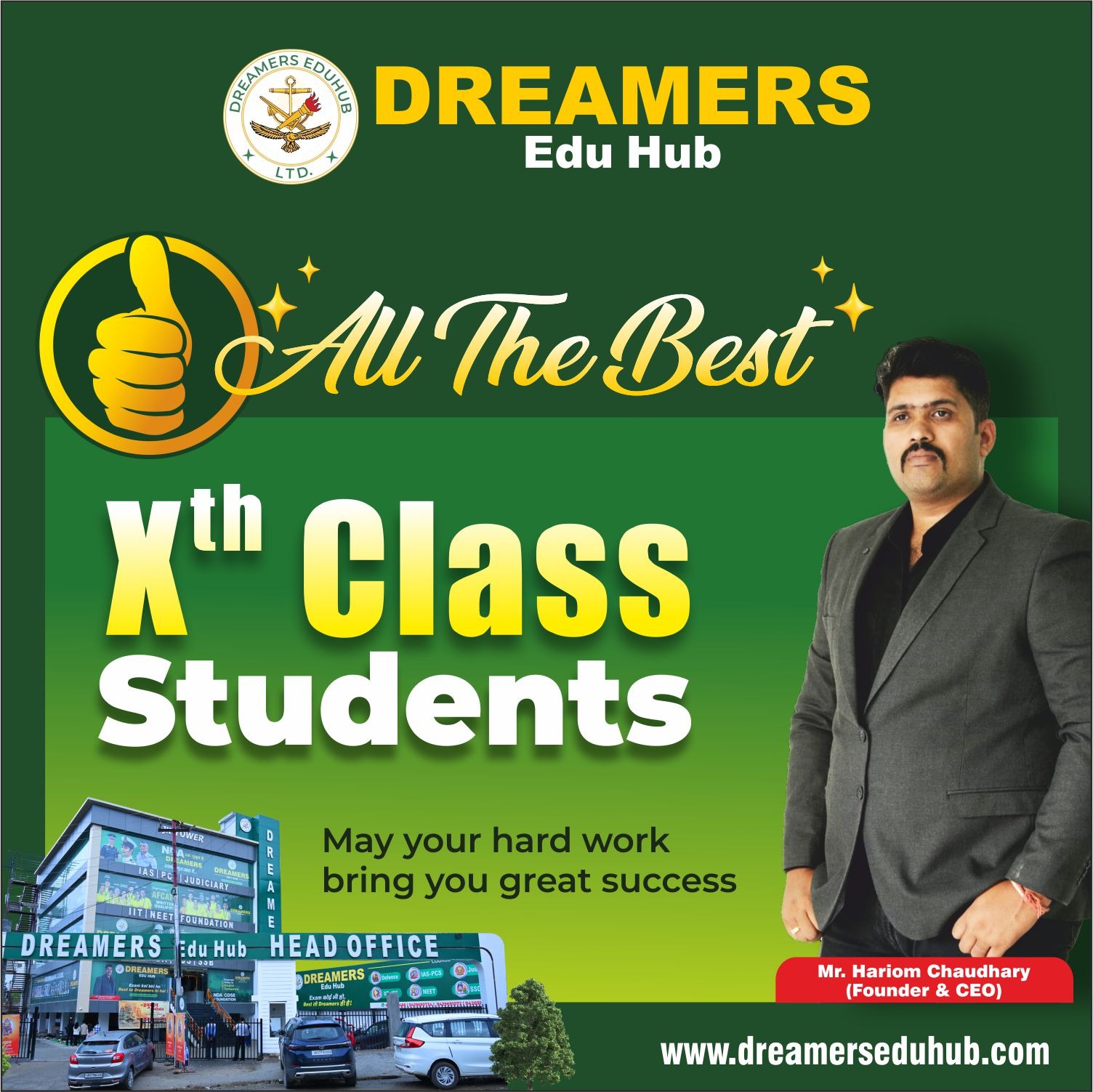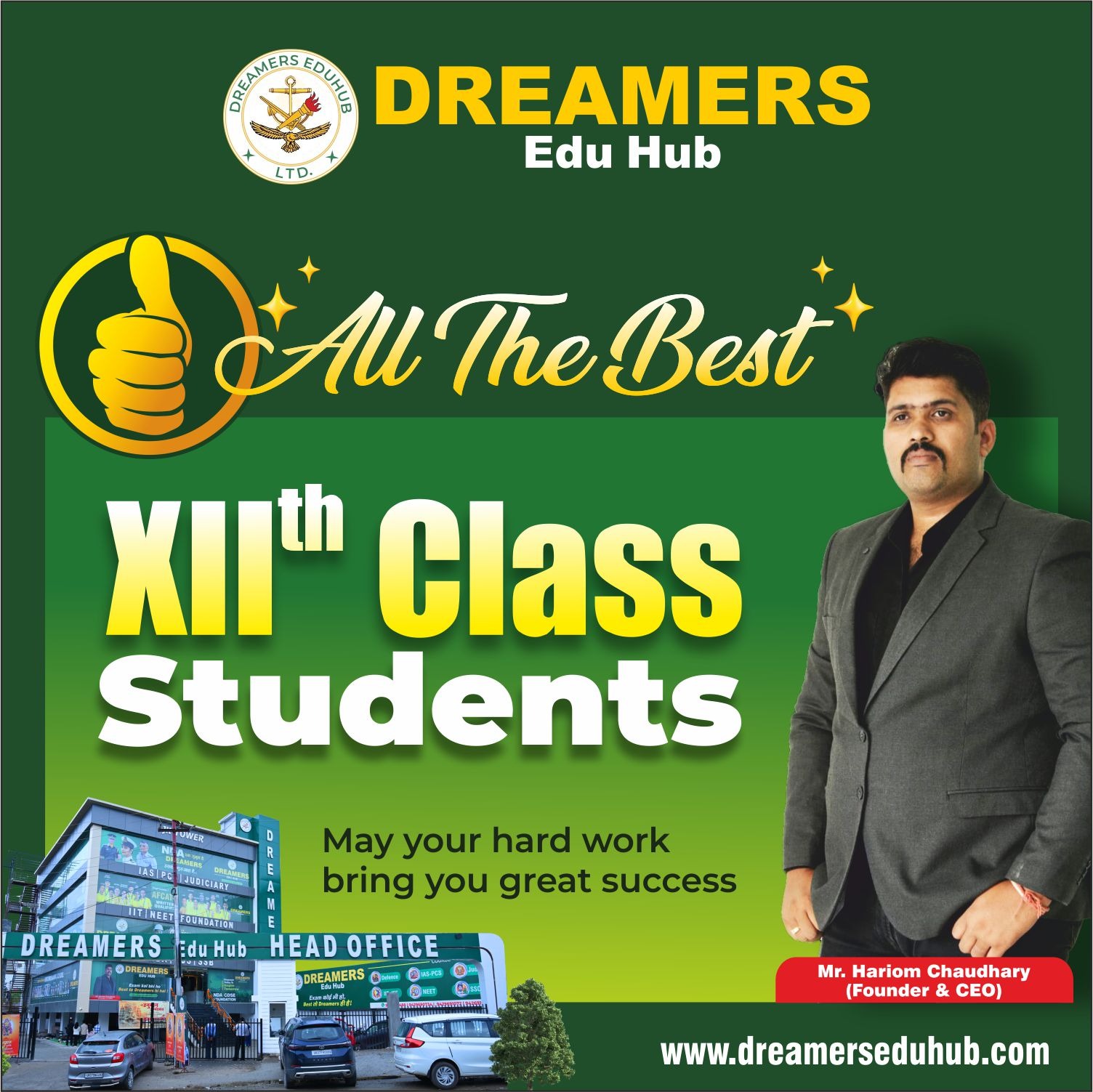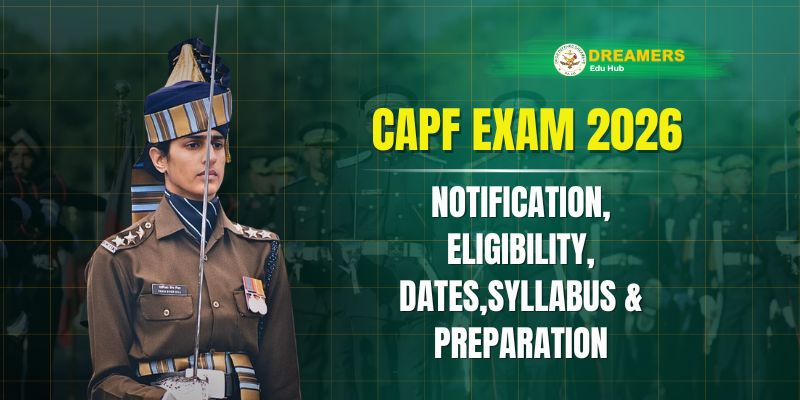क्यों Defence Research and Development Organisation ज़रूरी है?
जब हम अख़बारों या न्यूज़ में अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट सिस्टम या अर्जुन टैंक का नाम सुनते हैं, तो इनके पीछे चुपचाप काम करने वाला दिमाग होता है – Defence Research and Development Organisation।
यही वह संस्थान है जो भारत की सेनाओं के लिए
-
मिसाइल,
-
टैंक,
-
रडार,
-
ड्रोन,
-
आर्टिलरी गन,
-
नेवल सिस्टम
जैसी आधुनिक तकनीक तैयार करता है। सरल भाषा में कहें तो Defence Research and Development Organisation भारत की रक्षा–तकनीक की रीढ़ है। इसका मक़सद है कि भारत ज़रूरी हथियारों के लिए सिर्फ़ विदेशों पर निर्भर न रहे, बल्कि अपने देश में ही उन्हें डिज़ाइन और विकसित कर सके।
इस ब्लॉग में हम आसान हिन्दी में समझेंगे –
-
Defence Research and Development Organisation कब और कैसे बना,
-
इसकी संरचना और उद्देश्य क्या हैं,
-
DRDO द्वारा बनाई गई मुख्य मिसाइलें – अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, ब्रह्मोस,
-
ज़मीन पर इस्तेमाल होने वाले मुख्य सिस्टम – अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट, ATAGS तोप,
-
जीवन विज्ञान, नेवल और एयर सिस्टम,
-
चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा।
Defence Research and Development Organisation की स्थापना और शुरुआती सफ़र
Defence Research and Development Organisation की आधिकारिक स्थापना 1958 में हुई। यह कोई बिल्कुल नई संस्था नहीं थी, बल्कि तीन अलग–अलग इकाइयों को मिलाकर बनाई गई थी—
-
Defence Science Organisation (DSO)
-
Technical Development Establishments (TDEs) – जो सेना के लिए तकनीकी विकास करती थीं
-
Directorate of Technical Development and Production (DTDP)
इन सबको मिलाकर एक बड़ा वैज्ञानिक संगठन तैयार किया गया, जिसे आज हम Defence Research and Development Organisation, या संक्षेप में DRDO के नाम से जानते हैं।
शुरुआती समय में इसके पास लगभग दस लैबोरटरी थीं और काम भी ज़्यादातर बेसिक हथियार, विस्फोटक, सामग्री (materials) और छोटे–मोटे उपकरणों पर केंद्रित था। धीरे–धीरे DRDO ने अपने क्षेत्र और क्षमता दोनों का विस्तार किया।
महत्वपूर्ण पड़ाव:
-
1958–1970 – बुनियाद मज़बूत करने का समय, लैब स्थापित करना, वैज्ञानिकों की भर्ती, प्रारम्भिक शोध।
-
1980 के दशक – एक बड़ा कदम: Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) की शुरुआत, जिसने भारत की मिसाइल क्षमता को नई ऊँचाई दी।
-
1990–2000 – ज़्यादातर ध्यान मिसाइल, मुख्य युद्धक टैंक, रडार, टॉरपीडो, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर।
-
2010 के बाद – लंबी दूरी की मिसाइलें, ब्रह्मोस जैसी क्रूज़ मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, UAVs, नेटवर्क–सेंट्रिक वारफेयर, साइबर और स्पेस से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस।
आज Defence Research and Development Organisation के पास देश–भर में फैली हुई 50 से ज़्यादा लैब और प्रतिष्ठान हैं, जो अलग–अलग डोमेन – एरोनॉटिक्स, मिसाइल, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ़ साइंसेज़, मटीरियल्स और कॉम्बैट व्हीकल्स – में काम कर रहे हैं।
DRDO की संरचना, आदर्श वाक्य और लक्ष्य
Defence Research and Development Organisation का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित DRDO भवन है। यह सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है।
मुख्य बिंदु:
-
DRDO में कुल मिलाकर लगभग 30,000 कर्मचारी हैं, जिनमें क़रीब 5,000 वैज्ञानिक शामिल हैं।
-
लैबोरटरी देश के अलग–अलग शहरों – हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, देहरादून, चंडीगढ़, ग्वालियर, दिल्ली आदि – में फैली हैं।
-
हर लैब का अपना स्पेशल फोकस है – जैसे मिसाइल, एरोनॉटिक्स, नेवल सिस्टम, कॉम्बैट व्हीकल, आर्टिलरी, रडार, लाइफ़ साइंस इत्यादि।
मोटो (Adopted motto)
Defence Research and Development Organisation का आदर्श वाक्य है:
“Balasya Moolam Vigyanam” – Strength’s Origin is in Science
यानि असली ताक़त की जड़ विज्ञान में होती है। इसी सोच के साथ DRDO भारतीय सेना को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से लैस करने का काम करता है।
मुख्य उद्देश्य
-
भारत को महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाना
-
विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना
-
भारतीय परिस्थितियों – रेगिस्तान, पहाड़, हाई–एल्टीट्यूड, समुद्र, जंगल – के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करना
-
सेना, नौसेना और वायुसेना को समय–समय पर अपग्रेड और सपोर्ट देना
-
विकसित तकनीक को भारतीय सार्वजनिक और निजी उद्योगों को ट्रांसफ़र करना, ताकि बड़े पैमाने पर निर्माण भारत में हो सके
यही कारण है कि आज Defence Research and Development Organisation की बदौलत भारत सिर्फ़ आयातक नहीं, बल्कि कई मामलों में रक्षा उपकरणों का निर्यातक देश भी बन रहा है।
DRDO की प्रमुख मिसाइल प्रणालियाँ
मिसाइलें DRDO की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से हैं। 1980 के दशक में शुरू हुए Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) के तहत कई महत्त्वपूर्ण मिसाइलें बनीं। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों ने किया।
IGMDP के तहत पाँच मुख्य मिसाइलें विकसित की गईं:
-
Prithvi – सतह से सतह पर मार करने वाली बैटलफ़ील्ड मिसाइल
-
Agni – मध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की सीरीज़
-
Akash – सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल
-
Trishul – शॉर्ट रेंज SAM
-
Nag – एंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल
Prithvi मिसाइल
-
प्रकार: Surface-to-Surface Ballistic Missile
-
भूमिका: बैटलफील्ड में दुश्मन के ठिकानों पर प्रहार करना
-
रेंज: लगभग 150–250 किमी (वैरिएंट के अनुसार)
Prithvi भारत की शुरुआती स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक थी। इससे लॉकल स्तर पर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार करने की क्षमता मिली और Defence Research and Development Organisation की मिसाइल क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
Agni मिसाइल श्रृंखला
Agni परिवार भारत की रणनीतिक (Strategic) मिसाइल शक्ति की मुख्य रीढ़ है।
-
Agni-I – लगभग 700–900 किमी रेंज
-
Agni-II, III, IV, V – मध्यम से इंटर–कॉण्टिनेन्टल रेंज तक
-
मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती हैं
-
अलग–अलग प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं
Agni सीरीज़ की बदौलत भारत के पास विश्वसनीय न्युक्लियर डिटरेंस की क्षमता मानी जाती है। यह Defence Research and Development Organisation की सबसे चर्चित उपलब्धियों में गिना जाता है।
Akash मिसाइल
-
प्रकार: Medium Range Surface-to-Air Missile
-
भूमिका: दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि को मार गिराना
-
रेंज: लगभग 25–30 किमी (पुराने संस्करणों में, नए वैरिएंट में इससे ज़्यादा)
-
उपयोग: भारतीय वायुसेना और थलसेना दोनों के पास इसकी तैनाती है
Akash एक मोबाइल एयर–डिफेंस सिस्टम है, जिसके साथ रडार और कमांड कंट्रोल सिस्टम भी DRDO ने ही विकसित किए हैं।
Nag एंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल
-
प्रकार: तीसरी पीढ़ी की Anti-Tank Guided Missile (ATGM)
-
भूमिका: आधुनिक टैंकों और बख़्तरबंद वाहनों को नष्ट करना
-
वैरिएंट: ज़मीन–आधारित लॉन्चर (NAMICA), हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली Helina आदि
Nag मिसाइल “Fire and Forget” टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यानी निशाना लॉक होने के बाद ऑपरेटर को मिसाइल को गाइड नहीं करना पड़ता, मिसाइल खुद लक्ष्य तक पहुंचती है।
BrahMos – सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल
BrahMos को अक्सर Defence Research and Development Organisation की सबसे हाई–प्रोफ़ाइल उपलब्धियों में गिना जाता है।
-
प्रकार: Supersonic Cruise Missile
-
गति: लगभग Mach 3 (आवाज़ की गति से क़रीब तीन गुना)
-
रेंज: शुरुआती वर्ज़न में लगभग 290–350 किमी, नए वर्ज़न में इससे ज़्यादा
-
प्लेटफ़ॉर्म: जहाज़, पनडुब्बी, ज़मीन–आधारित लॉन्चर और Su-30MKI विमान से लॉन्च
-
विकास: भारत के DRDO और रूस की NPO Mashinostroyeniya के संयुक्त उपक्रम BrahMos Aerospace द्वारा
BrahMos की ख़ासियत:
-
सुपरसोनिक स्पीड, जिससे इंटरसेप्ट करना कठिन
-
Sea-skimming क्षमता – बेहद कम ऊँचाई पर उड़ते हुए लक्ष्य को हिट कर सकती है
-
भारी वॉरहेड और उच्च प्रिसीजन
BrahMos के कॉस्टल डिफेंस वर्ज़न को भारत ने फ़िलिपींस को निर्यात भी किया है, जो DRDO और Defence Research and Development Organisation के लिए बड़ा माइलस्टोन है।
ज़मीन पर ताक़त – टैंक, रॉकेट और तोपें
Arjun Main Battle Tank
Arjun MBT थलसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित मुख्य युद्धक टैंक है।
-
प्रोजेक्ट की शुरुआत: 1970 के दशक में
-
विकास: चेन्नई स्थित Combat Vehicles Research and Development Establishment (CVRDE) ने किया
-
सेना में शामिल: लगभग 2004 के आसपास
मुख्य विशेषताएँ:
-
120 mm राइफ़ल्ड गन, आधुनिक गोला–बारूद दागने में सक्षम
-
Kanchan Armour नामक स्वदेशी कम्पोज़िट कवच, जो उच्च स्तर की सुरक्षा देता है
-
आधुनिक Fire Control System, नाइट फ़ाइटिंग क्षमता, अच्छी मोबिलिटी
इसके अपग्रेडेड वर्ज़न Arjun Mk-1A में और ज़्यादा प्रोटेक्शन, बेहतर फ़ायरपावर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं।
Pinaka Multi-Barrel Rocket Launcher
Pinaka DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है।
-
कैलिबर: 214 mm
-
रेंज: Mark-I Enhanced में लगभग 45 किमी, Mark-II में इससे भी अधिक
-
क्षमता: एक बैटरी कुछ ही सेकंड में दर्जनों रॉकेट दुश्मन के क्षेत्र में दाग सकती है
-
उपयोग: कारगिल युद्ध में ऊँची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन ठिकानों को नष्ट करने में Pinaka की अहम भूमिका रही
Pinaka आज Defence Research and Development Organisation का ऐसा सिस्टम है जिसे कई मित्र देशों में निर्यात और परीक्षण के लिए भी देखा जा रहा है। इससे भारत की रॉकेट आर्टिलरी बहुत मज़बूत हुई है।
ATAGS – Advanced Towed Artillery Gun System
ATAGS एक आधुनिक 155 mm, 52-calibre towed howitzer है।
-
प्रोजेक्ट शुरुआत: लगभग 2013
-
विकास: पुणे की Armament Research and Development Establishment (ARDE) ने भारतीय निजी कंपनियों – Tata Advanced Systems, Bharat Forge आदि – के साथ मिलकर किया
-
रेंज: 45 किमी से अधिक, कुछ परीक्षणों में लगभग 48 किमी से भी ज़्यादा रेंज दिखाई गई
ख़ासियत:
-
पूरी तरह इलेक्ट्रिक ड्राइव – कम मेंटेनेंस और तेज़ ऑपरेशन
-
तेज़ “Shoot and Scoot” क्षमता – फ़ायर करके तुरंत पोज़िशन बदल सकती है
-
हाई रेट ऑफ़ फ़ायर – कम समय में कई राउंड दागने की क्षमता
ATAGS भारत को लंबी रेंज की आधुनिक आर्टिलरी क्षमता देता है और Defence Research and Development Organisation के “आत्मनिर्भर तोपख़ाना” विज़न को आगे बढ़ाता है।
नेवल, एयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
नेवल सिस्टम
भारतीय नौसेना के लिए DRDO ने कई महत्वपूर्ण सिस्टम विकसित किए हैं:
-
Varunastra जैसे हेवी वेट टॉरपीडो
-
आधुनिक Sonar और अंडरवॉटर सेंसर
-
जहाज़ों के लिए Anti-Submarine Warfare (ASW) सूट
-
फायर कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम
इनकी मदद से भारतीय नौसेना को समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों और जहाज़ों के ख़िलाफ़ मज़बूत क्षमता मिलती है।
एयरबोर्न सिस्टम और UAV
Defence Research and Development Organisation ने वायु क्षेत्र में भी बड़े प्रोजेक्ट किए हैं:
-
AEW&C “Netra” – एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो दुश्मन की गतिविधियों को दूर से देख सकता है
-
LCA Tejas प्रोजेक्ट में एवीओनिक्स, मटीरियल्स और वेपन इंटीग्रेशन में योगदान
-
Rustom/Tapas और अन्य UAV – निगरानी और इंटेलिजेंस के लिए
इन प्रोजेक्ट्स से भारतीय वायुसेना और अन्य एजेंसियों को Situational Awareness और नेटवर्क–सेंट्रिक वारफेयर की ताक़त मिलती है।
6.3 इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार और साइबर
आधुनिक युद्ध में रडार, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की भूमिका बहुत ज़्यादा है। DRDO ने:
-
ग्राउंड–बेस्ड, एयरबोर्न और शिप–बोर्न रडार
-
Electronic Warfare (EW) सिस्टम
-
सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क
-
साइबर और नेटवर्क–सिक्योरिटी से जुड़े टूल
जैसी तकनीकें विकसित की हैं। इससे भारतीय सेना दुश्मन को पहले देख सकती है, तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर सकती है और अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकती है।
लाइफ़ साइंस, सैनिकों की सुरक्षा और सपोर्ट सिस्टम
Defence Research and Development Organisation की एक अहम शाखा Life Sciences भी है, जो सीधे सैनिकों के स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ी है।
ये लैब्स:
-
ऊँचाई वाले इलाकों की फिज़ियोलॉजी पर रिसर्च करती हैं – जैसे सियाचिन में तैनात जवानों पर हाई–एल्टीट्यूड का प्रभाव
-
Special Rations और रेडी–टू–ईट फ़ूड पैकेट्स विकसित करती हैं
-
Extreme Cold Clothing, बुलेट–प्रूफ़ जैकेट, हेलमेट, बॉडी आर्मर डिज़ाइन करती हैं
-
NBC (Nuclear, Biological, Chemical) प्रोटेक्शन के लिए सूट, मास्क और डिटेक्टर बनाती हैं
इस तरह Defence Research and Development Organisation सिर्फ़ हथियार नहीं बनाता, बल्कि सैनिकों की जान बचाने और मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें सक्षम बनाने का काम भी करता है।
आत्मनिर्भर भारत, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट
काफी समय तक भारत हथियारों का बड़ा आयातक रहा है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है।
-
DRDO तकनीक विकसित करता है
-
Defence Research and Development Organisation इन तकनीकों को Defense Public Sector Units (DPSUs) और निजी कंपनियों को ट्रांसफ़र करता है
-
इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है
-
कुछ सिस्टम विदेशी मित्र देशों को भी निर्यात किए जाते हैं
BrahMos, Pinaka, रडार और आर्टिलरी सिस्टम जैसे उपकरणों में भारत ने एक्सपोर्ट की दिशा में अच्छा कदम बढ़ाया है। इससे एक तरफ़ रक्षा–आत्मनिर्भरता मज़बूत होती है, दूसरी तरफ़ विदेशी मुद्रा भी आती है और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि सुधरती है।
Defence Research and Development Organisation में करियर के अवसर
स्टूडेंट्स और डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए DRDO एक आकर्षक करियर विकल्प है।
मुख्य अवसर:
-
Scientist ‘B’ और अन्य वैज्ञानिक पद – इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले युवाओं के लिए
-
Technical Staff और Admin Staff – डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट के लिए
-
Junior Research Fellow (JRF), SRF, Research Associate – रिसर्च में रुचि रखने वाले PG और PhD स्टूडेंट्स के लिए
यहाँ काम करने वाले युवा:
-
अत्याधुनिक तकनीक पर काम करते हैं
-
सीधे–सीधे राष्ट्र रक्षा में योगदान देते हैं
-
सेना, नौसेना, वायुसेना और इंडस्ट्री के साथ करीबी तालमेल में प्रोजेक्ट्स करते हैं
इस तरह Defence Research and Development Organisation वैज्ञानिक प्रतिभा को देश सेवा से जोड़ता है।
चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा
इतने बड़े संगठन के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
-
कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ना
-
दुनिया में तेज़ी से बदलती तकनीक – AI, साइबर वारफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्वांटम टेक्नोलॉजी
-
स्टार्ट–अप और निजी उद्योग के साथ और तेज़ तालमेल की ज़रूरत
-
प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को लंबे समय तक जोड़कर रखना
इन चुनौतियों से निपटने के लिए Defence Research and Development Organisation:
-
प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ जॉइंट वेंचर और प्रोडक्शन पार्टनरशिप बढ़ा रहा है
-
स्टार्ट–अप्स के लिए इनोवेशन चैलेंज, iDEX जैसी योजनाओं में भाग लेता है
-
IIT, NIT और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स चला रहा है
-
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, एडवांस्ड रडार, स्पेस डिफेंस जैसे हाई–एंड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है
भविष्य में भारत की रक्षा–तकनीक कितनी मज़बूत और आत्मनिर्भर होगी, यह काफी हद तक Defence Research and Development Organisation की सफलता पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके हाथों में जो हथियार, टैंक, मिसाइल और सुरक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें डिज़ाइन करने का काम Defence Research and Development Organisation करता है।
मुख्य बातें याद रखने लायक:
-
DRDO, यानी Defence Research and Development Organisation, की स्थापना 1958 में हुई।
-
इसने Prithvi, Agni, Akash, Nag, BrahMos, Arjun Tank, Pinaka, ATAGS जैसी कई महत्वपूर्ण प्रणालियाँ विकसित कीं।
-
यह थलसेना, नौसेना और वायुसेना – तीनों को आधुनिक स्वदेशी तकनीक उपलब्ध कराता है।
-
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में Defence Research and Development Organisation की भूमिका केंद्रीय है; अब भारत कई सिस्टम अन्य देशों को भी निर्यात कर रहा है।
-
युवा वैज्ञानिकों और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए DRDO एक ऐसा मंच है जहाँ विज्ञान के माध्यम से देश सेवा का अवसर मिलता है।
इस तरह कहा जा सकता है कि Defence Research and Development Organisation वह “निरव शस्त्रागार” है जो भारत की रक्षा–ताक़त को विज्ञान, तकनीक और नवाचार के माध्यम से दिन–प्रतिदिन मज़बूत बना रहा है।